मैं इतना मसरूफ़ भी नहीं हूँ कि
शहर कि किसी गली में लड़ते हुए कुत्तों को खड़े होकर न देखूँ ।
शहर में लोग भी गाड़ी जैसे ही चलते हैं
एक ही ढ़र्रे पर चलते हैं।
शहर में लोगों के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई पड़ते
क्योंकि उनके चेहरे ही नहीं हैं ।
उनके चेहरे तरह तरह के मुखौटों से ढ़के रहते हैं।
शहर की रफ्तार ठीक एस्कलेटर जैसी है
सीढ़ी जैसी नहीं
सीढ़ी तो गाँव की आराम की ज़िंदगी की रफ्तार है।
एक दिन ये सारे पहिए रुक जाएँगे
रफ्तार का ईंधन खाली हो जाएगा
फिर खरीदी हुई पानी की बोतल की आखिरी बूंद को देखकर
गाँव के कुंए के पानी की स्वाभाविक विलासिता की याद आएगी।
जितना छोटा हमने दुनिया को कर दिया
उतने ही छोटे हम खुद हो गए हैं।
हम सिर्फ शहर की बेरूह आवाज़ जैसे
अंदर से खाली हो गए हैं।
लौटने के लिए अब कोई गाँव नहीं हैं
गाँव वही कीमती इंसानियत है
जिसको हम कीमत की खोज में गंवा चुके हैं।
---- संतोष कुमार काना
25th September, 2013, an evening at Kathmandu
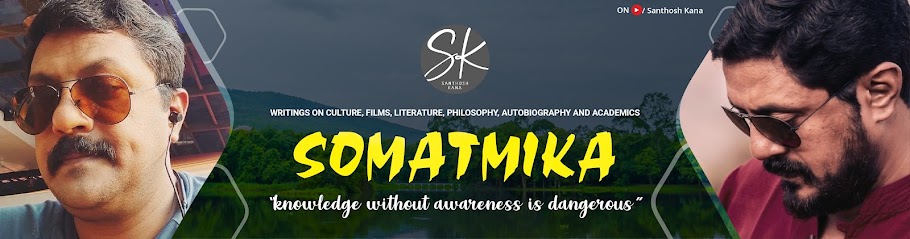

No comments:
Post a Comment